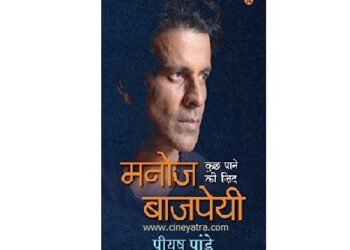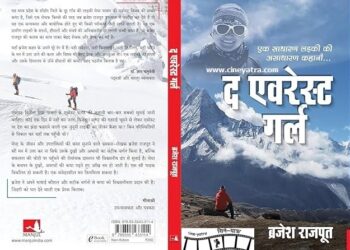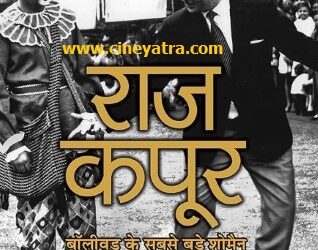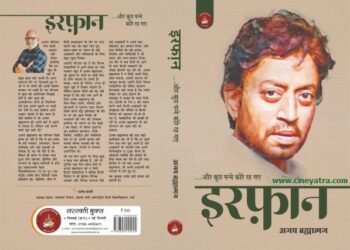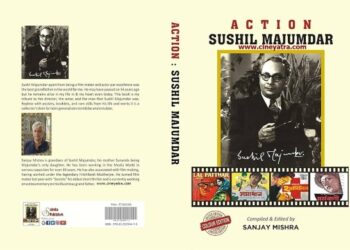-दीपक दुआ…
 जल-प्रलय के बाद पृथ्वी पानी में डूब चुकी है। सिर्फ वही जीव बचे हैं जिन्हें पानी में जीवित रहना आता है। लेकिन मछलियों, मगरमच्छों आदि के बीच इंसान का एक बच्चा भी बचा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जिसे कुदरत ने पानी के अंदर जीवित रहना सिखा दिया। उसे बचाया भी एक शार्क मछली ने। अब वह अपनी मछली मां और मछली दोस्तों के साथ समंदर के अंदर मखरी नामक नगर में रहता है। लेकिन इस दुनिया में भी छल-कपट, होड़-ईर्ष्या, लालच-द्वेष आदि हैं। बाकी सबसे अलग होने के कारण यह बच्चा ‘मानु’ कइयों को सुहाता भी नहीं है। और फिर एक दिन मखरी पर होता है एक भयंकर हमला।
जल-प्रलय के बाद पृथ्वी पानी में डूब चुकी है। सिर्फ वही जीव बचे हैं जिन्हें पानी में जीवित रहना आता है। लेकिन मछलियों, मगरमच्छों आदि के बीच इंसान का एक बच्चा भी बचा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जिसे कुदरत ने पानी के अंदर जीवित रहना सिखा दिया। उसे बचाया भी एक शार्क मछली ने। अब वह अपनी मछली मां और मछली दोस्तों के साथ समंदर के अंदर मखरी नामक नगर में रहता है। लेकिन इस दुनिया में भी छल-कपट, होड़-ईर्ष्या, लालच-द्वेष आदि हैं। बाकी सबसे अलग होने के कारण यह बच्चा ‘मानु’ कइयों को सुहाता भी नहीं है। और फिर एक दिन मखरी पर होता है एक भयंकर हमला।
 जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ‘पानी की दुनिया’ समुद्र के अंदर के जीवों की कहानी है। एक अलग किस्म का फैंटेसी संसार इस कहानी में उकेरा गया है। अपने फ्लेवर से यह कहानी रुडयार्ड किपलिंग की ‘द जंगल बुक’ सरीखी लगती है जिसमें इंसान के एक बच्चे को भेड़ियों ने पाला और वह बच्चा जंगल का होकर रह गया। वहां शेर खान उस बच्चे मोगली का दुश्मन था तो यहां मगरमच्छ मानु के पीछे पड़े हैं। जंगल बुक अगर जंगल की कहानी थी तो यह उपन्यास हमें पानी के नीचे की अनदेखी दुनिया में ले जाता है। उधर अपने कलेवर में यह कहानी हमें हॉलीवुड की फिल्मों की भी याद दिलाती है, खासतौर से एनिमेशन फिल्मों ‘फाईंडिंग नीमो’ व ‘फाईंडिंग डोरी’ की। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता भी है कि जैसे हम वैसी ही कोई एनिमेशन फिल्म देख रहे हैं। खास बात यह भी है कि इसकी भाषा भी उन फिल्मों के संवादों सरीखी है-सीधी, सरल, बिना किसी सजावट के यह भाषा एक आम पाठक को अपना बना लेती है और पहले ही पन्ने से वह इसे पढ़ते-पढ़ते अपने ज़ेहन में जो फिल्म देखनी शुरू करता है वह सीधे आखिरी पन्ने पर आकर ही खत्म होती है।
जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ‘पानी की दुनिया’ समुद्र के अंदर के जीवों की कहानी है। एक अलग किस्म का फैंटेसी संसार इस कहानी में उकेरा गया है। अपने फ्लेवर से यह कहानी रुडयार्ड किपलिंग की ‘द जंगल बुक’ सरीखी लगती है जिसमें इंसान के एक बच्चे को भेड़ियों ने पाला और वह बच्चा जंगल का होकर रह गया। वहां शेर खान उस बच्चे मोगली का दुश्मन था तो यहां मगरमच्छ मानु के पीछे पड़े हैं। जंगल बुक अगर जंगल की कहानी थी तो यह उपन्यास हमें पानी के नीचे की अनदेखी दुनिया में ले जाता है। उधर अपने कलेवर में यह कहानी हमें हॉलीवुड की फिल्मों की भी याद दिलाती है, खासतौर से एनिमेशन फिल्मों ‘फाईंडिंग नीमो’ व ‘फाईंडिंग डोरी’ की। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता भी है कि जैसे हम वैसी ही कोई एनिमेशन फिल्म देख रहे हैं। खास बात यह भी है कि इसकी भाषा भी उन फिल्मों के संवादों सरीखी है-सीधी, सरल, बिना किसी सजावट के यह भाषा एक आम पाठक को अपना बना लेती है और पहले ही पन्ने से वह इसे पढ़ते-पढ़ते अपने ज़ेहन में जो फिल्म देखनी शुरू करता है वह सीधे आखिरी पन्ने पर आकर ही खत्म होती है।
हिन्दी में स्तरीय फंतासी लेखन काफी कम होता है, न के बराबर। नई पीढ़ी के लेखकों में तो कोई विरला ही इस तरफ आगे बढ़ता है। ऐसे में जयपुर के युवा लेखक बंधु रॉइन रागा और रिझ्झम रागा का यह चौथा उपन्यास इस दिशा में न सिर्फ एक सार्थक कदम लगता है बल्कि यह उम्मीद भी जगाता है कि फंतासी लेखन के मामले में युवा लेखकों की झोली अभी खाली नहीं हुई है।
 इससे पहले के अपने उपन्यासों ‘मिख्ला’, ‘पंडित दलित’ और ‘राइट-मैन’ में अपनी लेखनी के विविध पहलू दिखा चुके रागा बंधुओं ने जीवन के 12 वर्ष अनाथालय में बिताए। अब वे अपनी उम्र के तीसरे दशक में हैं और जिस तरह का लेखन कर रहे हैं वह उन्हें जल्द ही भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। खासतौर से फंतासी लेखन के प्रति उनका रुझान उन्हें एक विशिष्टता प्रदान करता है। इस उपन्यास में दो-एक जगह शब्दों और वाक्य-विन्यास का हेरफेर ज़रा-सा खटकता है। कहीं-कहीं ऐसा भी लगता है कि घटनाएं पाठक के मन की दिशा में नहीं जा रही हैं लेकिन जल्दी ही वह सही लगने लगती हैं। उपन्यास खत्म होता है तो मन में कसक बाकी रह जाती है कि यह इतनी जल्दी क्यों खत्म हुआ। दुर्भाग्य ही है कि ऐसा लेखन अपने यहां ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसी पर हॉलीवुड वाले कोई फिल्म बना कर ले आएं तो हम ही लोग इसके स्वागत में कालीन बिछा देंगे। कलामोस प्रकाशन से आया यह उपन्यास मात्र 175 रुपए का है और अमेजन के इस लिंक पर उपलब्ध है।
इससे पहले के अपने उपन्यासों ‘मिख्ला’, ‘पंडित दलित’ और ‘राइट-मैन’ में अपनी लेखनी के विविध पहलू दिखा चुके रागा बंधुओं ने जीवन के 12 वर्ष अनाथालय में बिताए। अब वे अपनी उम्र के तीसरे दशक में हैं और जिस तरह का लेखन कर रहे हैं वह उन्हें जल्द ही भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। खासतौर से फंतासी लेखन के प्रति उनका रुझान उन्हें एक विशिष्टता प्रदान करता है। इस उपन्यास में दो-एक जगह शब्दों और वाक्य-विन्यास का हेरफेर ज़रा-सा खटकता है। कहीं-कहीं ऐसा भी लगता है कि घटनाएं पाठक के मन की दिशा में नहीं जा रही हैं लेकिन जल्दी ही वह सही लगने लगती हैं। उपन्यास खत्म होता है तो मन में कसक बाकी रह जाती है कि यह इतनी जल्दी क्यों खत्म हुआ। दुर्भाग्य ही है कि ऐसा लेखन अपने यहां ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसी पर हॉलीवुड वाले कोई फिल्म बना कर ले आएं तो हम ही लोग इसके स्वागत में कालीन बिछा देंगे। कलामोस प्रकाशन से आया यह उपन्यास मात्र 175 रुपए का है और अमेजन के इस लिंक पर उपलब्ध है।
 (दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिजाज़ से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)
(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिजाज़ से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)