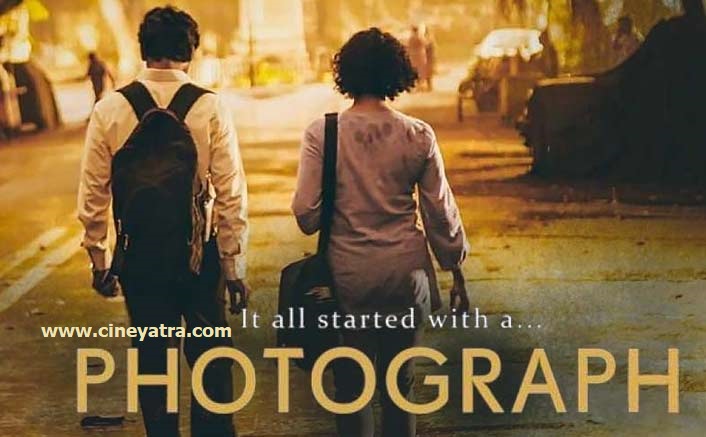-दीपक दुआ… (This review is featured in IMDb Critics Reviews)  ‘मैडम, बरसों बाद जब आप यह फोटो देखेंगी तो आपको अपने चेहरे पर यही धूप दिखाई देगी…।’ मैडम तो फोटो खिंचवा कर चली गई। गांव में बैठी अपनी दादी को बहलाने के लिए फोटोग्राफर ने इसी मैडम की तस्वीर दादी को भेज दी कि मैंने अपने लिए यह लड़की पसंद कर रखी है। उसी वक्त पीछे ‘नूरी’ फिल्म का गाना बज रहा था, सो लड़की का नाम भी बता दिया-नूरी। लेकिन दादी गांव से उठ कर सीधे मुंबई आ धमकी-मिलवाओ नूरी से। फोटोग्राफर के कहने पर मैडम मान गई, दादी से मिलती रही और कहानी आगे चलती रही।
‘मैडम, बरसों बाद जब आप यह फोटो देखेंगी तो आपको अपने चेहरे पर यही धूप दिखाई देगी…।’ मैडम तो फोटो खिंचवा कर चली गई। गांव में बैठी अपनी दादी को बहलाने के लिए फोटोग्राफर ने इसी मैडम की तस्वीर दादी को भेज दी कि मैंने अपने लिए यह लड़की पसंद कर रखी है। उसी वक्त पीछे ‘नूरी’ फिल्म का गाना बज रहा था, सो लड़की का नाम भी बता दिया-नूरी। लेकिन दादी गांव से उठ कर सीधे मुंबई आ धमकी-मिलवाओ नूरी से। फोटोग्राफर के कहने पर मैडम मान गई, दादी से मिलती रही और कहानी आगे चलती रही। ‘लंचबॉक्स’ के बाद डायरेक्टर रितेश बत्रा अमेरिका जाकर दो फिल्में बना आए हैं। उन्हें अलग तरह से कहानी कहने का शौक है। बल्कि ऐसा लगता है कि वह कहानी नहीं कहते, कहानी को जान-बूझ कर खुला छोड़ देते हैं कि वह खुद अपने रास्ते तलाशे। ‘लंचबॉक्स’ भी ऐसी ही थी। उसकी नायिका को खुशी की तलाश थी। इसकी नायिका भी उदास है। कपड़े, कैरियर, जीवनसाथी, सब उसके माता-पिता उसके लिए चुन रहे हैं और वह चुपचाप उनकी बात मानती जा रही है। लेकिन इस फोटोग्राफर की प्रेमिका की एक्टिंग करते-करते वह बदलने लगती है। यह बदलाव आक्रामक नहीं है। लेकिन उसके भीतर अरमान जागने लगते हैं। उसे वह बचपन वाली कैंपा कोला चाहिए जो उसके दादा जी उस दिलवाते थे। वह अपनी नौकरानी के गांव जाना चाहती है क्योंकि वहां बहुत शांति है। अपनी फोटो में वह खुद को ज्यादा खुश, ज्यादा सुंदर पाती है। फोटोग्राफर के साथ उठते-बैठते उसे महसूस होने लगता है कि वह सचमुच पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा सुंदर हो गई है।
‘लंचबॉक्स’ के बाद डायरेक्टर रितेश बत्रा अमेरिका जाकर दो फिल्में बना आए हैं। उन्हें अलग तरह से कहानी कहने का शौक है। बल्कि ऐसा लगता है कि वह कहानी नहीं कहते, कहानी को जान-बूझ कर खुला छोड़ देते हैं कि वह खुद अपने रास्ते तलाशे। ‘लंचबॉक्स’ भी ऐसी ही थी। उसकी नायिका को खुशी की तलाश थी। इसकी नायिका भी उदास है। कपड़े, कैरियर, जीवनसाथी, सब उसके माता-पिता उसके लिए चुन रहे हैं और वह चुपचाप उनकी बात मानती जा रही है। लेकिन इस फोटोग्राफर की प्रेमिका की एक्टिंग करते-करते वह बदलने लगती है। यह बदलाव आक्रामक नहीं है। लेकिन उसके भीतर अरमान जागने लगते हैं। उसे वह बचपन वाली कैंपा कोला चाहिए जो उसके दादा जी उस दिलवाते थे। वह अपनी नौकरानी के गांव जाना चाहती है क्योंकि वहां बहुत शांति है। अपनी फोटो में वह खुद को ज्यादा खुश, ज्यादा सुंदर पाती है। फोटोग्राफर के साथ उठते-बैठते उसे महसूस होने लगता है कि वह सचमुच पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा सुंदर हो गई है।
 किस्सों से ज्यादा यह किरदारों की फिल्म है। मुंबई शहर तो इसका एक अहम किरदार है ही। उस कमरे में लगा वह पंखा भी अपनी मौजूदगी का अहसास कराता है जिसमें रफी अपने साथियों के साथ रहता है और जिस पर लटक कर एक दिन तिवारी जी चल बसे थे। रफी के ये साथी, इन सब की पूरबिया बोली में बातें, लटक कर मरे तिवारी जी, कैंपा वाले पारसी अंकल की चुप्पी, बैकग्राउंड में बजते पुराने फिल्मी गाने, ये तमाम चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। साउंड रिकॉर्डिंग खासी ज़बर्दस्त है। कैमरा बड़ी ही सफाई से एक खिड़की बन जाता है जिसमें से आप इस फिल्म के भीतर झांकते हैं।
किस्सों से ज्यादा यह किरदारों की फिल्म है। मुंबई शहर तो इसका एक अहम किरदार है ही। उस कमरे में लगा वह पंखा भी अपनी मौजूदगी का अहसास कराता है जिसमें रफी अपने साथियों के साथ रहता है और जिस पर लटक कर एक दिन तिवारी जी चल बसे थे। रफी के ये साथी, इन सब की पूरबिया बोली में बातें, लटक कर मरे तिवारी जी, कैंपा वाले पारसी अंकल की चुप्पी, बैकग्राउंड में बजते पुराने फिल्मी गाने, ये तमाम चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। साउंड रिकॉर्डिंग खासी ज़बर्दस्त है। कैमरा बड़ी ही सफाई से एक खिड़की बन जाता है जिसमें से आप इस फिल्म के भीतर झांकते हैं। फोटोग्राफर रफी के किरदार में नवाज़ुद्दीन सिद्दिकी बखूबी समाए हैं। चौंकाती तो सान्या मल्होत्रा हैं। मिलोनी के शांत किरदार में वह भावहीन भले ही लगती हों लेकिन उनका यही भाव ही आपको उनसे जोड़ता है। इच्छा होती है कि उनके बारे में और जाना जाए। उसके पिता बने सचिन खेडेकर, नौकरानी बनीं गीतांजलि कुलकर्णी, रफी के साथियों में आकाश सिन्हा जैसे तमाम कलाकार अपने किरदारों को भरपूर जीते हैं। लेकिन पर्दे पर रंगत बिखेरती हैं रफी की दादी बनीं फर्रुख जफर। जब भी वह दिखाई-सुनाई देती हैं, आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पातें। वैसे बता दूं कि यह वही अदाकारा हैं जो बरसों पहले ‘उमराव जान’ में रेखा की मां बनी थीं।
फोटोग्राफर रफी के किरदार में नवाज़ुद्दीन सिद्दिकी बखूबी समाए हैं। चौंकाती तो सान्या मल्होत्रा हैं। मिलोनी के शांत किरदार में वह भावहीन भले ही लगती हों लेकिन उनका यही भाव ही आपको उनसे जोड़ता है। इच्छा होती है कि उनके बारे में और जाना जाए। उसके पिता बने सचिन खेडेकर, नौकरानी बनीं गीतांजलि कुलकर्णी, रफी के साथियों में आकाश सिन्हा जैसे तमाम कलाकार अपने किरदारों को भरपूर जीते हैं। लेकिन पर्दे पर रंगत बिखेरती हैं रफी की दादी बनीं फर्रुख जफर। जब भी वह दिखाई-सुनाई देती हैं, आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पातें। वैसे बता दूं कि यह वही अदाकारा हैं जो बरसों पहले ‘उमराव जान’ में रेखा की मां बनी थीं।
 फिल्म की रफ्तार धीमी है। कहीं-कहीं सीन काफी लंबे लगने लगते हैं। फिल्म का अंत भी अचानक से आ जाता है। लगता है जैसे डायरेक्टर ने आपको पटरी से लाकर किसी खुले मैदान में छोड़ दिया हो। फिल्म की एक कमी यह भी है कि यह आपके भीतर अरमान तो जगाती है लेकिन आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती। इस किस्म का सिनेमा फिल्म समारोहों में ज्यादा सराहा जाता है। आम दर्शकों के लिए इसमें ज्यादा कुछ भले न हो, लेकिन सिनेमा को समझने, उसे दिलों में सहेजने के शौकीनों को यह फिल्म भाएगी।
फिल्म की रफ्तार धीमी है। कहीं-कहीं सीन काफी लंबे लगने लगते हैं। फिल्म का अंत भी अचानक से आ जाता है। लगता है जैसे डायरेक्टर ने आपको पटरी से लाकर किसी खुले मैदान में छोड़ दिया हो। फिल्म की एक कमी यह भी है कि यह आपके भीतर अरमान तो जगाती है लेकिन आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती। इस किस्म का सिनेमा फिल्म समारोहों में ज्यादा सराहा जाता है। आम दर्शकों के लिए इसमें ज्यादा कुछ भले न हो, लेकिन सिनेमा को समझने, उसे दिलों में सहेजने के शौकीनों को यह फिल्म भाएगी।
अपनी रेटिंग-तीन स्टार
Release Date-15 March, 2019
 (दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)
(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)