-दीपक दुआ… (This review is featured in IMDb Critics Reviews)
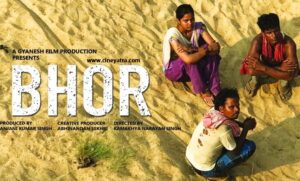 मुसहर-बिहार में समाज के हाशिये पर बैठी एक ऐसी जनजाति जिसे अछूत माना जाता है। घनघोर गरीबी में रहने को अभिशप्त ये लोग चूहा (मूषक) मार कर खाने के चलते ‘मुसहर’ कहे गए। इसी समाज की दसवीं में पढ़ रही बुधनी का ब्याह चमकू के बेटे सुगन के संग हो गया। फाकामस्ती में जी रहे इस परिवार के न कोई सपने और न ही उन्हें हासिल करने का कोई संघर्ष। लेकिन बुधनी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दसवीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। जिलाधीश ने बुला कर ईनाम मांगने को कहा तो बोली-शौचालय बनवा दीजिए। लेकिन जल्द ही वह पति संग मजदूरी करने दिल्ली आ गई। मगर यहां भी वही हाल कि सब लोग रेल की पटरियों पर ही जाते।
मुसहर-बिहार में समाज के हाशिये पर बैठी एक ऐसी जनजाति जिसे अछूत माना जाता है। घनघोर गरीबी में रहने को अभिशप्त ये लोग चूहा (मूषक) मार कर खाने के चलते ‘मुसहर’ कहे गए। इसी समाज की दसवीं में पढ़ रही बुधनी का ब्याह चमकू के बेटे सुगन के संग हो गया। फाकामस्ती में जी रहे इस परिवार के न कोई सपने और न ही उन्हें हासिल करने का कोई संघर्ष। लेकिन बुधनी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दसवीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। जिलाधीश ने बुला कर ईनाम मांगने को कहा तो बोली-शौचालय बनवा दीजिए। लेकिन जल्द ही वह पति संग मजदूरी करने दिल्ली आ गई। मगर यहां भी वही हाल कि सब लोग रेल की पटरियों पर ही जाते।
 रंजन चौहान, कामाख्या नारायण सिंह और भास्कर विश्वनाथन की टीम ने फिल्म को कायदे से लिखा है। मुसहरों की जीवन-शैली और उनकी सोच को करीब से दिखाती है यह फिल्म। छोटे-छोटे संवादों और दृश्यों के ज़रिए इस ‘सूखे’ विषय में भी रोचकता बनाने की सफल कोशिश की गई है। बड़ा काम निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने किया है जिन्होंने फिल्म को ‘फिल्म’ की बजाय सच्चाई के इतने करीब रखा है कि यह पर्दे पर चल रही सच्ची कहानी लगती है। हर सीन उन्होंने बेहद जानदार रखा है। उनके रिसर्च पर, उनके कल्पनाशीलता पर गर्व होता है।
रंजन चौहान, कामाख्या नारायण सिंह और भास्कर विश्वनाथन की टीम ने फिल्म को कायदे से लिखा है। मुसहरों की जीवन-शैली और उनकी सोच को करीब से दिखाती है यह फिल्म। छोटे-छोटे संवादों और दृश्यों के ज़रिए इस ‘सूखे’ विषय में भी रोचकता बनाने की सफल कोशिश की गई है। बड़ा काम निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने किया है जिन्होंने फिल्म को ‘फिल्म’ की बजाय सच्चाई के इतने करीब रखा है कि यह पर्दे पर चल रही सच्ची कहानी लगती है। हर सीन उन्होंने बेहद जानदार रखा है। उनके रिसर्च पर, उनके कल्पनाशीलता पर गर्व होता है।
 फिल्म में हर चीज़ इस कदर वास्तविक है कि इसे देखते हुए आप हैरान हो सकते हैं। कलाकारों के फटे-पुराने कपड़ों से लेकर टूटी-फूटी झुग्गियों और यहां तक कि ताश के घिसे हुए पत्तों तक का ध्यान रखा गया है। फिल्म के किरदार जहां रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं, लगता ही नहीं कि ये लोग वास्तविक मुसहर नहीं बल्कि पेशेवर एक्टर हैं। तमाम कलाकारों ने कमाल का काम भी किया है। चमकू बने नलनीश नील ने गज़ब ढाया है। ताड़ी पीने, खाना खाने, कीचड़ में गिरने जैसे तमाम दृश्यों में उन्होंने वास्तविकता की हद पार की है। सुगन बने देवेश रंजन हों, कम बोलने वाली बुधनी बनी सावेरी गौड़ या कोई भी दूसरा कलाकार, हर किसी का काम सटीक, सधा हुआ रहा है। दो-एक गाने हैं जो बेहतरीन हैं। पार्श्व-संगीत, लोकेशंस, कैमरा, सब सधा हुआ है। लेकिन…!
फिल्म में हर चीज़ इस कदर वास्तविक है कि इसे देखते हुए आप हैरान हो सकते हैं। कलाकारों के फटे-पुराने कपड़ों से लेकर टूटी-फूटी झुग्गियों और यहां तक कि ताश के घिसे हुए पत्तों तक का ध्यान रखा गया है। फिल्म के किरदार जहां रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं, लगता ही नहीं कि ये लोग वास्तविक मुसहर नहीं बल्कि पेशेवर एक्टर हैं। तमाम कलाकारों ने कमाल का काम भी किया है। चमकू बने नलनीश नील ने गज़ब ढाया है। ताड़ी पीने, खाना खाने, कीचड़ में गिरने जैसे तमाम दृश्यों में उन्होंने वास्तविकता की हद पार की है। सुगन बने देवेश रंजन हों, कम बोलने वाली बुधनी बनी सावेरी गौड़ या कोई भी दूसरा कलाकार, हर किसी का काम सटीक, सधा हुआ रहा है। दो-एक गाने हैं जो बेहतरीन हैं। पार्श्व-संगीत, लोकेशंस, कैमरा, सब सधा हुआ है। लेकिन…!
 गरीबी, अशिक्षा, छूआछूत, बेरोज़गारी, पलायन, शौचालय की ज़रूरत, संघर्ष की ताकत, मीडिया की सार्थकता की बात करती यह फिल्म क्लाइमैक्स से पहले तक जिस सहज बहाव में चल रही होती है, अंत आते-आते थोड़ी अजीब-सी हो जाती है। जल्दी से सब कुछ समेटने लगती है और जिस तरह से समेटती है, वह कुछ अधूरा-सा लगता है। बावजूद इसके इसे देखा जाना चाहिए। बिना उपदेशात्मक हुए समाज के एक ऐसे वर्ग के बारे में बहुत कुछ कहती है यह जिसके बारे में सिनेमा तो छोड़िए, हमारा समाज भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता।
गरीबी, अशिक्षा, छूआछूत, बेरोज़गारी, पलायन, शौचालय की ज़रूरत, संघर्ष की ताकत, मीडिया की सार्थकता की बात करती यह फिल्म क्लाइमैक्स से पहले तक जिस सहज बहाव में चल रही होती है, अंत आते-आते थोड़ी अजीब-सी हो जाती है। जल्दी से सब कुछ समेटने लगती है और जिस तरह से समेटती है, वह कुछ अधूरा-सा लगता है। बावजूद इसके इसे देखा जाना चाहिए। बिना उपदेशात्मक हुए समाज के एक ऐसे वर्ग के बारे में बहुत कुछ कहती है यह जिसके बारे में सिनेमा तो छोड़िए, हमारा समाज भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता।
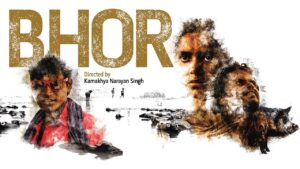 इस किस्म की फिल्मों को ‘फेस्टिवल सिनेमा’ कहा जाता है। ये फिल्में कुछ एक फिल्म समारोहों में जाती हैं, प्रबुद्ध वर्ग की वाहवाही के साथ थोड़े-बहुत ईनाम-इकराम, वाहवाही पाकर डिब्बों में बंद होकर रह जाती हैं। यह फिल्म तो गोआ के अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अलावा देश-विदेश में कई जगह सराही गई। अब ओ.टी.टी. की आवक ने ज़माना बदल दिया है जिसके चलते यह दर्शकों तक भी पहुंच पा रही है। एम.एक्स. प्लेयर ऐप पर इसे मुफ्त में देखा जा सकता है।
इस किस्म की फिल्मों को ‘फेस्टिवल सिनेमा’ कहा जाता है। ये फिल्में कुछ एक फिल्म समारोहों में जाती हैं, प्रबुद्ध वर्ग की वाहवाही के साथ थोड़े-बहुत ईनाम-इकराम, वाहवाही पाकर डिब्बों में बंद होकर रह जाती हैं। यह फिल्म तो गोआ के अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अलावा देश-विदेश में कई जगह सराही गई। अब ओ.टी.टी. की आवक ने ज़माना बदल दिया है जिसके चलते यह दर्शकों तक भी पहुंच पा रही है। एम.एक्स. प्लेयर ऐप पर इसे मुफ्त में देखा जा सकता है।
(रेटिंग की ज़रूरत ही क्या है? रिव्यू पढ़िए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हां, इस रिव्यू पर अपने विचार ज़रूर बताएं।)
Release Date-05 February, 2021
 (दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)
(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)









