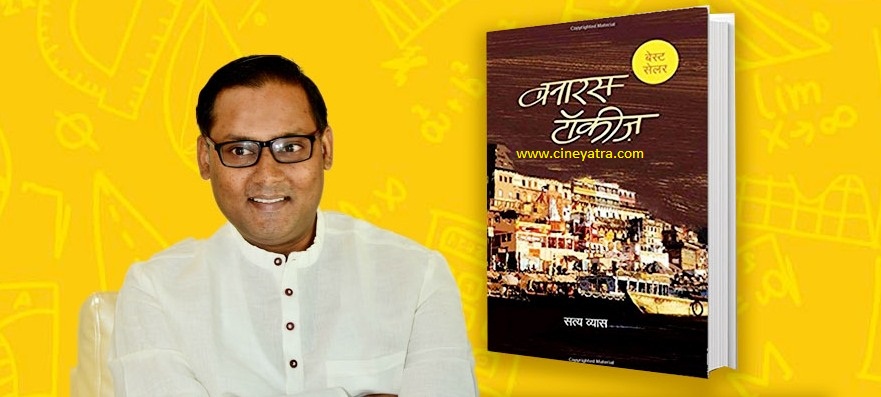-दीपक दुआ…
हिन्दी साहित्य के फैलते बाजार के चहेते लेखक हैं सत्य व्यास। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी यानी बी.एच.यू. से लॉ की पढ़ाई करने और वहां के भगवान दास होस्टल में रहने के अपने अनुभवों को एक कहानी की शक्ल देकर वह 2015 में ‘बनारस टॉकीज़’ जैसा बैस्ट-सैलर उपन्यास लिख चुके हैं। उनका नया उपन्यास ‘दिल्ली दरबार’ हाल ही में आया है। पिछले दिनों सत्य व्यास ‘साहित्य आज तक’ में शिरकत करने के लिए दिल्ली में थे। उनसे एक लंबी अंतरंग बातचीत हुई जिसके प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं-
-‘बनारस टॉकीज़’ को पढ़ते समय लगता है कि इस उपन्यास में जो भी घटनाएं और किरदार हैं, वे सब सचमुच वहां ऐसे ही हुए होंगे। आपके मुताबिक इस कहानी में कितना सच और कितनी कल्पना है?
-काफी सारा सच है और थोड़ी कल्पना भी। जैसे अगर रैगिंग वाले एपिसोड की बात करें तो वह पूरे का पूरा काल्पनिक है क्योंकि बी.एच.यू. में रैगिंग की परंपरा है ही नहीं। लेकिन यह मुझे इसलिए दिखानी पड़ी क्योंकि जो तीन प्रमुख पात्र हैं उनकी दोस्ती यहीं से प्रगाढ़ होती है। इसके अलावा बाकी सब कहीं न कहीं सच है। एक और बात है कि मेरी हमेशा से ही यह सोच रही है कि किसी कहानी में मुख्य पात्र कम होने चाहिएं ताकि पाठक बीस किरदारों को पढ़ कर उलझ न जाए। तो वहां मेरे आसपास के जो बीस किरदार थे और उनकी जो खूबियां थीं वे मैंने इन तीनों में डाल दीं।
-‘बनारस टॉकीज़’ पढ़ते समय ऐसा भी लगता है कि हम किसी मनोरंजक हिन्दी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इस उपन्यास की समीक्षाओं में भी यह बात सामने आई थी कि इस पर एक शानदार फिल्म बनाई जा सकती है, खासतौर से ‘3 ईडियट्स’ का सीक्वेल। क्या किसी ने आपसे इस बारे में संपर्क किया?
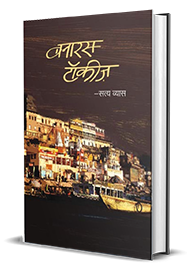 -हां, ऐसी बातें उस समय हुई थीं और उसके बाद कई फिल्मकारों ने मुझसे इस बारे में बात भी की। लेकिन बात इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि कोई इस पर टी.वी. सीरियल बनाने की बात करता है तो किसी ने वेब-सीरिज की बात की। एक-दो लोगों ने छोटे बजट की फिल्म बनाने का ऑफर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसी कहानी है जिस पर बड़े सितारों को लेकर एक बड़े बजट की फिल्म बनेगी तो वह ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और उसे काफी पसंद भी किया जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं इस इंतजार में हूं कि किसी बड़े बैनर या बड़े निर्देशक की नजर में यह कहानी आ जाए।
-हां, ऐसी बातें उस समय हुई थीं और उसके बाद कई फिल्मकारों ने मुझसे इस बारे में बात भी की। लेकिन बात इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि कोई इस पर टी.वी. सीरियल बनाने की बात करता है तो किसी ने वेब-सीरिज की बात की। एक-दो लोगों ने छोटे बजट की फिल्म बनाने का ऑफर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसी कहानी है जिस पर बड़े सितारों को लेकर एक बड़े बजट की फिल्म बनेगी तो वह ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और उसे काफी पसंद भी किया जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं इस इंतजार में हूं कि किसी बड़े बैनर या बड़े निर्देशक की नजर में यह कहानी आ जाए।
-अपने अगले उपन्यास ‘दिल्ली दरबार’ के बारे में बताएं?
-पहली बात तो यह कि यह दिल्ली की कहानी नहीं है बल्कि यह दिल्ली में एक कहानी है। अपनी ही लिखी दो लाइनें कहता हूं-‘था लोगों से सुना यह है शहर बड़ा दिल्ली, खानाबदोश थे हम आना ही पड़ा दिल्ली।’ यह एक ऐसा शहर है जो बाहर के लोगों को लगातार बुलाता, आकर्षित करता रहा है और पूरे प्यार और एहतराम से रखता आया है। इस शहर ने कभी किसी को दुर्भाव से नहीं देखा। सात बार उजड़ी है दिल्ली लेकिन इसने कभी किसी से यह नहीं कहा कि जाओ यहां से। पहले मैंने इसका नाम भी ‘सराय दिल्ली’ रखा था। यह कहानी बाहर से आए उन लड़कों की है जो अच्छी पढ़ाई और अच्छे रोजगार के लालच में दिल्ली आते हैं और बाहर से आए लड़कों की एक अपनी अलग ही मस्ती होती है। उनकी मस्ती, उनका प्यार, पढ़ाई जैसी बातें हैं इसमें, और जैसा कि ‘बनारस टॉकीज़’ में भी था, मैंने इस कहानी को एक थ्रिल से भी जोड़ा है। कहानी 2011 में खत्म होती है जब भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। उस वर्ल्ड कप से एक थ्रिल को जोड़ा गया है जो अंत में जाकर खुलता है।
-यानी ‘बनारस टॉकीज़’ जैसी ही एक और मस्ती भरी कहानी। आपने कुछ ज्यादा गंभीर लिखने के बारे में नहीं सोचा?
 -वह भी लिखूंगा लेकिन चूंकि यह मेरी दूसरी ही किताब है तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गंभीर होना ठीक नहीं था क्योंकि पाठकों के मन में अभी ‘बनारस टॉकीज़’ बैठी हुई है तो मुझे लगा कि अभी वह मुझसे वैसी ही खिलंदड़ेपन वाली कहानी की ही उम्मीद करेंगे। साथ ही मुझे लगता था कि अभी मेरे लेखन में वह परिपक्वता नहीं आई है कि मैं कुछ गंभीर लिखता।
-वह भी लिखूंगा लेकिन चूंकि यह मेरी दूसरी ही किताब है तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गंभीर होना ठीक नहीं था क्योंकि पाठकों के मन में अभी ‘बनारस टॉकीज़’ बैठी हुई है तो मुझे लगा कि अभी वह मुझसे वैसी ही खिलंदड़ेपन वाली कहानी की ही उम्मीद करेंगे। साथ ही मुझे लगता था कि अभी मेरे लेखन में वह परिपक्वता नहीं आई है कि मैं कुछ गंभीर लिखता।
-‘बनारस टॉकीज़’ में आपने बनारस शहर को भी एक किरदार के तौर पर पेश किया है। क्या ‘दिल्ली दरबार’ में भी ऐसा होगा?
-जी बिल्कुल। यह कहानी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ही है। दिल्ली इसके नायक को एक जगह खड़े होकर देख रही है। वह उसे बढ़ते हुए देखती है और एक जगह आकर वह उसे छोड़ देती है कि मैं यहीं हूं, अब तुम जाओ। मैं फिर कहना चाहूंगा कि यह कहानी दिल्ली में है, दिल्ली की नहीं है। और जिस तरह से ‘बनारस टॉकीज़’ पूरे बनारस की कहानी नहीं कहता उसी तरह से ‘दिल्ली दरबार’ पूरी दिल्ली की कहानी नहीं है।
-क्या उम्मीद है आपको इस किताब से?
-मुझे लगता है कि अगर पाठक इसमें बताए गए थ्रिल के साथ खुद को जोड़ पाएंगे तो यह किताब बेहद पसंद की जाएगी और अगर वे इस थ्रिल के साथ खुद को नहीं जोड़ पाए तो शायद इसे उतना पसंद नहीं किया जा सकेगा जितना ‘बनारस टॉकीज़’ को किया गया। लेकिन मुझे यह किताब लिख कर बहुत मजा आया और इस किताब के आने के बाद मैं खुद को एक ‘लेखक’ कह पाऊंगा, जो अभी तक मैं खुद को नहीं कहता हूं।
-ऐसा क्यों, ‘बनारस टॉकीज़’ तो आपका हिट उपन्यास है?
-ऐसा इसलिए कि ‘बनारस टॉकीज़’ में मैंने जो लिखा है उसका अधिकांश हिस्सा मैंने जिया है या मेरे आसपास घटा है। उसमें एक लेखक की कल्पना बहुत कम है जबकि ‘दिल्ली दरबार’ लगभग पूरे का पूरा एक लेखक की कल्पना से उपजी हुई, बुनी हुई कहानी है।
-एक लेखक को आप कब सफल मानते हैं?
-मेरे उपन्यास का कोई भी पेज पढ़ते समय अगर किसी पाठक को यह लगे कि यह तो बोर कर रहा है तो मैं असफल हूं। अगर किसी को यह लगे कि यह तीन पेज छोड़ कर आगे चला जाए तो मैं असफल हूं। बतौर लेखक मेरी सफलता ही तब है जब मैं पढ़ने वाले को एकदम शुरू से ही बांध लूं और लगातार उसे बांधे रखूं। ‘बनारस टॉकीज़’ में ऐसा ही था और मैं यकीन दिलाता हूं कि ‘दिल्ली दरबार’ में भी आपको ऐसा ही मिलेगा।
-अपने यहां या तो गंभीर साहित्य आता रहा या फिर लुगदी कहा जाने वाला लोकप्रिय साहित्य। लेकिन इधर इन दोनों के बीच में एक मध्यमार्गी साहित्य आने लगा है जो आप और आपके कई समकालीन लेखक लिख रहे हैं और चेतन भगत इस धारा के अगुआ हैं। इस धारा के उभरने की आप क्या वजह मानते हैं?
 -देखिए, पहली बात तो यह कि मैं इस किस्म के वर्गीकरण को नहीं मानता। मैं एक ही समय में ‘गुनाहों का देवता’ को गंभीर भी मानता हूं और लोकप्रिय भी। मैं एक ही समय में ‘आपका बंटी’ को गंभीर भी मानता हूं और लोकप्रिय भी। लेकिन इनमें कहीं न कहीं भाषा ऐसी कलिष्ट हो जाया करती थी कि पाठक का पठन वहीं थम जाता था। जब चेतन भगत आए तो उन्होंने अपने लेखन को इतना सहज और सरल कर दिया कि हम जैसे कई लोगों को लगने लगा कि हम भी लिख सकते हैं। इससे पहले जितनी भी कहानियां आ रही थीं वे अस्सी के दशक की थीं जबकि इधर समय बदला है, पाठक बदले हैं, उनका रहन-सहन बदला है लेकिन लेखक नहीं बदला। उसके लेखन में न ई-मेल आया न मोबाइल, न फेसबुक। लेखक यह समझे ही नहीं कि समाज बदल रहा है तो हमें भी अपने लेखन को बदलना है। चेतन भगत ने यह काम बखूबी किया और यही वजह है कि युवा पीढ़ी के पाठकों ने उन्हें हाथोंहाथ लिया।
-देखिए, पहली बात तो यह कि मैं इस किस्म के वर्गीकरण को नहीं मानता। मैं एक ही समय में ‘गुनाहों का देवता’ को गंभीर भी मानता हूं और लोकप्रिय भी। मैं एक ही समय में ‘आपका बंटी’ को गंभीर भी मानता हूं और लोकप्रिय भी। लेकिन इनमें कहीं न कहीं भाषा ऐसी कलिष्ट हो जाया करती थी कि पाठक का पठन वहीं थम जाता था। जब चेतन भगत आए तो उन्होंने अपने लेखन को इतना सहज और सरल कर दिया कि हम जैसे कई लोगों को लगने लगा कि हम भी लिख सकते हैं। इससे पहले जितनी भी कहानियां आ रही थीं वे अस्सी के दशक की थीं जबकि इधर समय बदला है, पाठक बदले हैं, उनका रहन-सहन बदला है लेकिन लेखक नहीं बदला। उसके लेखन में न ई-मेल आया न मोबाइल, न फेसबुक। लेखक यह समझे ही नहीं कि समाज बदल रहा है तो हमें भी अपने लेखन को बदलना है। चेतन भगत ने यह काम बखूबी किया और यही वजह है कि युवा पीढ़ी के पाठकों ने उन्हें हाथोंहाथ लिया।
-अब आगे क्या लिखने जा रहे हैं?
-शुरूआत हो चुकी है। मेरी अगली कहानी है ‘चौरासी’ जिसके 80-90 पेज मैं लिख चुका हूं। जब सन् 84 में सिक्खों का कत्लेआम हुआ था तो हम बोकारो में थे और मैं काफी छोटा था। नानावटी आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा कत्लेआम दिल्ली में हुआ और उसके बाद बोकारो में। लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग है। यह मारने की कहानी नहीं है, यह बचाने की कहानी है। उस खून-खराबे के दौर में भी जो कहीं प्यार बचा था, कहीं मानवता बची थी, यह उसकी बात करती है। जो हो रहा है वह भी दिखाती है लेकिन साथ ही यह एक ऐसे लड़के की कहानी कहती है जो एक सिक्ख परिवार को बचाने में लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि साल भर में मैं इसे तैयार कर लूंगा।
(interview-November, 2016)
 (दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)
(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)